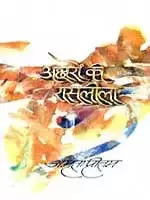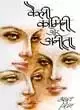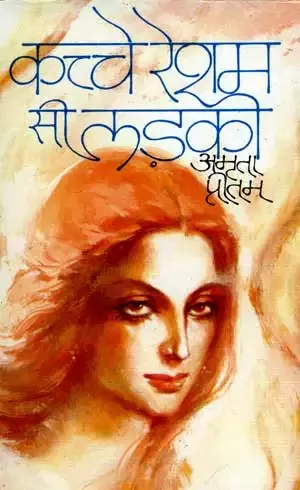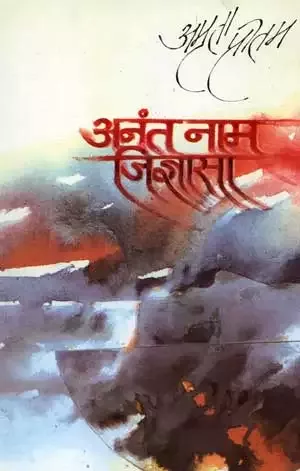|
लेख-निबंध >> अक्षरों की रासलीला अक्षरों की रासलीलाअमृता प्रीतम
|
555 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है अमृता प्रीतम का उत्कृष्ट आलेख...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
घर, क़बीला, समाज, मज़हब और सिसायत भी हमारे चाँद-सूरज होते हैं, और इनको
लगे ग्रहण के वक़्त जब किसी शायर, आशिक और दरवेश का जन्म होता है तो यह
हकीकत है कि दर्द का मोती उसके मस्तक में पड़ जाता है...
चेतना की यात्रा बहुत लम्बी होती है-
घर, क़बीले को जब टूटते रिश्तों का ग्रहण लगता है, तो जिस चेतना का जन्म होता है, उसके दर्द की इन्तहाँ अपनी तरह की होती है..
समाज को जब तरह-तरह की नाइन्साफ़ियों का ग्रहण लगता है, तो चेतना के अहसास की शिद्दत अपनी तरह की होती है..
मज़हब के चाँद को जब फ़िरक़ापरस्ती का ग्रहण लगता है, तो आसमान की आत्मा कैसे तड़पती है,यह चेतना अपनी तरह की होती है...
और सिसायत के सूरज को जब सत्ता की हवस का ग्रहण लगता है, तो धरती की आत्मा कैसे बिलखती है, यह चेतना अपनी तरह की होती है..
दुनिया के अदबी इतिहास को दर्द के मोती मिलते हैं, पर कोई नहीं जानता कि किसी कलमवाले की चेतना को ज़िन्दगी के कितने ग्रहण देखने और झेलने पड़ते हैं....
चेतना की यात्रा बहुत लम्बी होती है-
घर, क़बीले को जब टूटते रिश्तों का ग्रहण लगता है, तो जिस चेतना का जन्म होता है, उसके दर्द की इन्तहाँ अपनी तरह की होती है..
समाज को जब तरह-तरह की नाइन्साफ़ियों का ग्रहण लगता है, तो चेतना के अहसास की शिद्दत अपनी तरह की होती है..
मज़हब के चाँद को जब फ़िरक़ापरस्ती का ग्रहण लगता है, तो आसमान की आत्मा कैसे तड़पती है,यह चेतना अपनी तरह की होती है...
और सिसायत के सूरज को जब सत्ता की हवस का ग्रहण लगता है, तो धरती की आत्मा कैसे बिलखती है, यह चेतना अपनी तरह की होती है..
दुनिया के अदबी इतिहास को दर्द के मोती मिलते हैं, पर कोई नहीं जानता कि किसी कलमवाले की चेतना को ज़िन्दगी के कितने ग्रहण देखने और झेलने पड़ते हैं....
श्रुति परम्परा
प्राचीन भारत में श्रुति-परम्परा की छाप इतनी गहरी थी कि प्राचीन ऋषियों
के चिन्तन को लिखाई में उतारना किसी को मंजूर नहीं था।
वेदों के सूक्त आवाज़ की जिस अदायगी से उचारे जाते थे वह अदायगी सिर्फ़ श्रुति-परम्परा से ही क़ायम रखी जा सकती थी। इसलिए उन्हें भोजपत्रों पर, कपड़े पर या पत्थरों पर की लिखाई में नहीं उतारा गया।
यह फ़िक्र पहली बार बौद्धों और जैनियों को हुआ था कि चिन्तनशील बुजुर्गों के न रहने पर अयोग्य पात्र के हाथ पड़ने से यह चिन्तन खो जायगा। अगर सब कुछ लिखावट में हो तो खो नहीं पायेगा।
इतिहास मिलता है कि बौद्ध चिन्तन को सोने के पत्रों पर अंकित किया गया था और उन प्राचीन पत्रों पर चित्रकारी भी की गयी थी।
वेदों के पैरोकार फिर भी अपने निश्चय पर बने रहे, श्रुति-परम्परा से जुड़े हुए। लेकिन मुहम्मद गौरी हमले के वक़्त जब शहर और मंदिर तबाह होने लगे, लगा कि पूरी परम्परा खो जायगी तब वो श्रुति-परम्परा से कलमी परंपरा की ओर आये। लेकिन वह कैलीग्राफी के पहलू से एक हज़ार साल पीछे रह गये थे। खैर, श्रुति-साहित्य को कलमी सूरत मिली और बाद में पन्द्रहवीं-सोलहवीं सदी में उस साहित्य को सजा-सँवारकर पेश करने का वक़्त आया।
प्राचीन पत्ता लिखाईवाला चित्रित बौद्ध चिन्तन कुछ इसलिए बच गया कि तुर्क़ हमलावारों के वक़्त बौद्ध संन्यासी वो पाण्डुलिपियाँ नेपाल में ले गये।
प्राचीन पत्तालिखाई वाला चित्रित जैन चिन्तन भी इसीलिए बच गया कि जैन मुनि वो पाण्डुलिपियाँ दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के उन मंदिरों में ले गये थे, जहाँ उनकी हिफा़ज़त के बहुत मज़बूत भंडार थे।
वेदों के सूक्त आवाज़ की जिस अदायगी से उचारे जाते थे वह अदायगी सिर्फ़ श्रुति-परम्परा से ही क़ायम रखी जा सकती थी। इसलिए उन्हें भोजपत्रों पर, कपड़े पर या पत्थरों पर की लिखाई में नहीं उतारा गया।
यह फ़िक्र पहली बार बौद्धों और जैनियों को हुआ था कि चिन्तनशील बुजुर्गों के न रहने पर अयोग्य पात्र के हाथ पड़ने से यह चिन्तन खो जायगा। अगर सब कुछ लिखावट में हो तो खो नहीं पायेगा।
इतिहास मिलता है कि बौद्ध चिन्तन को सोने के पत्रों पर अंकित किया गया था और उन प्राचीन पत्रों पर चित्रकारी भी की गयी थी।
वेदों के पैरोकार फिर भी अपने निश्चय पर बने रहे, श्रुति-परम्परा से जुड़े हुए। लेकिन मुहम्मद गौरी हमले के वक़्त जब शहर और मंदिर तबाह होने लगे, लगा कि पूरी परम्परा खो जायगी तब वो श्रुति-परम्परा से कलमी परंपरा की ओर आये। लेकिन वह कैलीग्राफी के पहलू से एक हज़ार साल पीछे रह गये थे। खैर, श्रुति-साहित्य को कलमी सूरत मिली और बाद में पन्द्रहवीं-सोलहवीं सदी में उस साहित्य को सजा-सँवारकर पेश करने का वक़्त आया।
प्राचीन पत्ता लिखाईवाला चित्रित बौद्ध चिन्तन कुछ इसलिए बच गया कि तुर्क़ हमलावारों के वक़्त बौद्ध संन्यासी वो पाण्डुलिपियाँ नेपाल में ले गये।
प्राचीन पत्तालिखाई वाला चित्रित जैन चिन्तन भी इसीलिए बच गया कि जैन मुनि वो पाण्डुलिपियाँ दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के उन मंदिरों में ले गये थे, जहाँ उनकी हिफा़ज़त के बहुत मज़बूत भंडार थे।
दस्तावेज़
1982 में मारग्रेट थैचर और इंदिरा गाँधी की सरपरस्ती में जो
‘फ़ैस्टिवल ऑफ़ इण्डिया’ हुआ था, उस समय ब्रिटिश
लाइब्रेरी की
ओर से एक किताब तैयार करायी गयी थी, उस फ़ैस्टिवल को एक तोहफ़ा देने के
लिए। वह एक बहुत कीमती दस्तावेज़ है—THE ART OF THE BOOK IN
INDIA
BY JEREMIAH P.POSTY.
इस किताब में प्राचीन लिखाई के रंगीन चित्र भी दिये हुए हैं और उक्त के हालात भी।
पत्ता लिखाईवाली तमिल पाण्डुलिपियों के नमूने से लेकर जैन-बौद्ध पाण्डुलिपियों के चित्र भी दिये हैं।
प्राचीन पाण्डुलिपियों में घटनाओं के चित्र भी दिये जाते थे, जैसे-महावीर के जन्म के समय रानी त्रिशला अपने चौदह सपने सुना रही है, और उक्त के आलिम उन सपनों की ताबीर बता रहे हैं। इसी तरह हरिनेगनेशी नाम के देवता ने देवअनन्दा का गर्भ कैसे चुराया था, रानी त्रिशला की कोख में रखने के लिए।
अरब और ईरान से आयी कैलीग्राफ़ी का प्रभाव भारत की कला पर कितना हुआ इसकी तफ़सील से गुज़रते हुए इस पुस्तक में मुग़लराज के समय की चित्रकला का इतिहास भी सँभाला हुआ था। इतिहास के दिलचस्प हवालों में से कुछ यहाँ दर्ज़ करती हूँ।
‘कल्पसूत्र’ जैन चिन्तन की पुस्तक है जिसकी चित्रित लिखाई पन्द्रहवीं सदी में हुई थी। इसकी तैयारी गुजरात में हुई और चित्रों के लिए सोने और सीपियों का चूर्ण इस्तेमाल किया गया।
‘सिन्धबाद नामा’ सिन्धबाद की कहानियों की फ़ारसी किताब है जिसके लिखने का कोई नाम पता नहीं मिलता और किताब कब लिखी गयी है, वह समय भी नहीं मिलता। पहले सोचा जाता था कि शीरीज कला की मिसाल यह किताब वहीं कहीं लिखी गयी होगी लेकिन उसके रहने के लिए अपना घर भारत में मिला। लेकिन अब कला की बारीकियों से अनुमान होता है कि यह भारत में ही चित्रित हुई थी। इस नायाब किताब की कोई और प्रति कहीं और नहीं मिलती। शीरीज़ की कला तो ज़ाहिरा दिखाई देती है लेकिन किरदारों के लिबास दक्षिण भारत के हैं। गलों में लंबे और आगे से खुले चोगे कमरबन्द बँधे हुए।
मुग़ल दरबार के अलावा उस समय सिर्फ गोलकुण्डा का दरबार था, जहाँ ईरान की परम्परा भी थी और अहमदनगर-बीजापुर नगर की परंपरा थी।
‘शाहनामा’ फिरदौसी की उस लंबी कविता का नाम है जो ईरान के बादशाहों की ज़िन्दगी के हालात पेश करती है। यह पुस्तक गज़नी के महमूद की सरपरस्ती में तैयार हुई थी, आलीशान चित्रों के साथ। इसकी कई प्रतियाँ बनायी गईं थीं और लगता है कि एक प्रति भारत में तैयार हुयी थी। चौदह सौ तीस की इस प्रति में हैरात के शहज़ादे की लिखी हुई एक भूमिका है जिससे पता चलता है कि फिरदौसी ने एक बार गज़नी के महमूद से डरकर दिल्ली के बादशाह की पनाह ली थी और बादशाह ने बहुत कीमती तोहफे देकर उसे अपने वतन भिजवा दिया था। यहीं से अनुमान होता है कि ‘शाहनामा’ की एक प्रतिलिपि भारत में ही तैयार हुई थी।
एक और सबूत मिलता है कि भारत में तैयार की गयी प्रतिलिपि के चित्रों में वह पीला रंग इस्तेमाल किया गया है जो सिर्फ बंगाल के एक गाँव में बनाया जाता था। वह पीला रंग गोमूत्र से बनता था और इसके लिए केवल वही गायें ली जाती थीं जिन्हें आम के पत्ते खिलाए जाते थे।
सोलहवीं शताब्दी के मध्य में भारत मुसव्वरखानों की हालत बिखरी हुई थी। चाहे कई पुस्तकें बंगाल, माडू और गोलकुण्डा के कलाकारों के हाथों चित्रित हुई थीं।
राजपूत दरबार में संस्कृत और हिन्दी की कई पाण्डुलिपियाँ चित्रित हुई थीं और जैन चित्र उसी तरह गुजरात और राजस्थान में बन रहे थे। उस समय बादशाह अकबर ने कलाकारों के लिए बहुत बड़ा स्थान तैयार करवाया और कलाकार दूर-दूर से आगरा आने लगे, भारत की राजधानी में।
अकबर के इस बहुत बड़े ‘तस्वीरखाना’ में से जो पहली किताब तैयार हुई वह थी—तोतीनामा।
अकबर की सरपरस्ती में जो बहुत बड़ा काम हुआ, वह था—हमज़ानामा। यह हजरत मोहम्मद के चाचा अमीरहमज़ा के जंगी कारनामों की दास्तान है जो चौदह जिल्दों में तरतीब दी गयी। हर जिल्द में एक सौ चित्र थे। यह सूती कपड़े के टुकड़ों पर चित्रित की गई थी और इसे मुकम्मल सूरत देते हुए पन्द्रह बरस लगे।
‘जरीन-कलम़’ का अर्थ है सुनहरी कलम। यह एक किताब थी जो अकबर बादशाह ने कैलीग्राफी़ के माहिर एक कलाकार मुहम्मद हुसैन अल कश्मीरी को दी गई थी।
‘अम्बरी क़लम़’ भी एक किताब थी जो अकबर ने अब्दुल रहीम को दिया था। महाभारत, रामायण, हरिवंश, योगवाशिष्ठ और अथर्ववेद जैसे कई ग्रंथों का फारसी से अनुवाद भी बादशाह अकबर ने कराया था।
‘रज़म-नामा’ महाभारत फारसी अनुवाद का नाम है जिसका अनुवाद विद्वान ब्राह्मणों की मदद से बदायूँनी जैसे इतिहासकारों ने किया था, पन्द्रह सौ बयासी में और उसे फारसी के शायर फ़ैजी ने शायराना जुबान दी थी।
‘राज कुँवर’ किसी हिन्दू कहानी को लेकर फ़ारसी में लिखी हुई किताब है जिसके लेखक ने गुमनाम रहना पसंद किया था। इसकी इक्यावन पेण्टिंग सलीम के इलाहाबाद वाले तस्वीर खाने में तैयार हुई थीं।
‘बादशानामा’ शाहजहाँ के राज को लेकर अफदाल क़रीम लाहौरी की लिखी हुई वह किताब है जो औरंगजेब की बगावत ने पूरी नहीं होने दी थी।
‘ख़बरनामा’ इब्न हसन की लिखी हुई अली के कारनामों को बयान करती पुस्तक है जिसकी प्रतिलिपि मूलचन्द मुलतानी ने तैयार की थी। इसमें एक सौ छत्तीस मिनिएचर्स (भित्तिचित्र) हैं जो अफदाल हकीम मुल्तानी ने तैयार किये थे। मुल्तान में तैयार हुई इस पुस्तक के चित्रों के लिए बहुत-सा सोना और चाँदी इस्तेमाल किया गया था।
‘कारनामा-ए-इश्क़’ लाहौर के एक खत्री राय आनन्दराम की फ़ारसी में लिखी हुई किताब थी जिसके चित्र बनाते हुए उस वक़्त के मशहूर कलाकार गोवर्धन को पाँच साल लगे थे।
‘दस्तूर ए हिम्मत’ 1685 में लिखी हुई मुहम्मद मुराद की किताब थी जिसमें अवध के राजा कामरूप की और सीलोन की शहजादी कामलता की कहानी है। जिन्हें सपनों में एक दूसरे का दीदार हुआ था। राजा उसे खोजता हुआ आखिर सीलोन पहुँच जाता है और कामलता भी कामरूप को पहचान लेती है। इसकी चित्रकारी मुर्शिदाबाद में हुई, 1760 में। हर पृष्ठ पर बहुत सा सोना इस्तेमाल किया गया।
‘रागमाला’ के चित्रण में मुगल की दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मुगल दरबार के राजपूतों ओहदेदारों के कारण आगरा के तस्वीर खाने में यह पुस्तक तैयार हुई जिसमें रागों के परिवारों का ब्यौरा है। हर राग की पाँच पत्नियाँ (रागिनियाँ), और आगे उनके राग पुत्र हैं।
ब्रिटिश लाईब्रेरी लन्दन में देवचित्रों की दो एलबम हैं, जिनके चौंसठ चित्र अठारहवीं सदी के आखिर में लखनऊ के कलाकारों ने तैयार किये थे। हर चित्र के हाशिये पर सोने-चाँदी के पत्ते बनाये गये थे। ये दो एलबम दो लाख सड़सठ हज़ार एक सौ अठ्ठावन पौण्ड में बिके थे।
अठारहवीं शताब्दी के खत्म होने पर हस्तलिपियों की पाण्डुलिपियाँ बनाने की परम्परा भी खत्म हो गयी। तब कलकत्ता में प्रेस लग गया था जिसने किताबों की सूरत बदल दी।
इस किताब में प्राचीन लिखाई के रंगीन चित्र भी दिये हुए हैं और उक्त के हालात भी।
पत्ता लिखाईवाली तमिल पाण्डुलिपियों के नमूने से लेकर जैन-बौद्ध पाण्डुलिपियों के चित्र भी दिये हैं।
प्राचीन पाण्डुलिपियों में घटनाओं के चित्र भी दिये जाते थे, जैसे-महावीर के जन्म के समय रानी त्रिशला अपने चौदह सपने सुना रही है, और उक्त के आलिम उन सपनों की ताबीर बता रहे हैं। इसी तरह हरिनेगनेशी नाम के देवता ने देवअनन्दा का गर्भ कैसे चुराया था, रानी त्रिशला की कोख में रखने के लिए।
अरब और ईरान से आयी कैलीग्राफ़ी का प्रभाव भारत की कला पर कितना हुआ इसकी तफ़सील से गुज़रते हुए इस पुस्तक में मुग़लराज के समय की चित्रकला का इतिहास भी सँभाला हुआ था। इतिहास के दिलचस्प हवालों में से कुछ यहाँ दर्ज़ करती हूँ।
‘कल्पसूत्र’ जैन चिन्तन की पुस्तक है जिसकी चित्रित लिखाई पन्द्रहवीं सदी में हुई थी। इसकी तैयारी गुजरात में हुई और चित्रों के लिए सोने और सीपियों का चूर्ण इस्तेमाल किया गया।
‘सिन्धबाद नामा’ सिन्धबाद की कहानियों की फ़ारसी किताब है जिसके लिखने का कोई नाम पता नहीं मिलता और किताब कब लिखी गयी है, वह समय भी नहीं मिलता। पहले सोचा जाता था कि शीरीज कला की मिसाल यह किताब वहीं कहीं लिखी गयी होगी लेकिन उसके रहने के लिए अपना घर भारत में मिला। लेकिन अब कला की बारीकियों से अनुमान होता है कि यह भारत में ही चित्रित हुई थी। इस नायाब किताब की कोई और प्रति कहीं और नहीं मिलती। शीरीज़ की कला तो ज़ाहिरा दिखाई देती है लेकिन किरदारों के लिबास दक्षिण भारत के हैं। गलों में लंबे और आगे से खुले चोगे कमरबन्द बँधे हुए।
मुग़ल दरबार के अलावा उस समय सिर्फ गोलकुण्डा का दरबार था, जहाँ ईरान की परम्परा भी थी और अहमदनगर-बीजापुर नगर की परंपरा थी।
‘शाहनामा’ फिरदौसी की उस लंबी कविता का नाम है जो ईरान के बादशाहों की ज़िन्दगी के हालात पेश करती है। यह पुस्तक गज़नी के महमूद की सरपरस्ती में तैयार हुई थी, आलीशान चित्रों के साथ। इसकी कई प्रतियाँ बनायी गईं थीं और लगता है कि एक प्रति भारत में तैयार हुयी थी। चौदह सौ तीस की इस प्रति में हैरात के शहज़ादे की लिखी हुई एक भूमिका है जिससे पता चलता है कि फिरदौसी ने एक बार गज़नी के महमूद से डरकर दिल्ली के बादशाह की पनाह ली थी और बादशाह ने बहुत कीमती तोहफे देकर उसे अपने वतन भिजवा दिया था। यहीं से अनुमान होता है कि ‘शाहनामा’ की एक प्रतिलिपि भारत में ही तैयार हुई थी।
एक और सबूत मिलता है कि भारत में तैयार की गयी प्रतिलिपि के चित्रों में वह पीला रंग इस्तेमाल किया गया है जो सिर्फ बंगाल के एक गाँव में बनाया जाता था। वह पीला रंग गोमूत्र से बनता था और इसके लिए केवल वही गायें ली जाती थीं जिन्हें आम के पत्ते खिलाए जाते थे।
सोलहवीं शताब्दी के मध्य में भारत मुसव्वरखानों की हालत बिखरी हुई थी। चाहे कई पुस्तकें बंगाल, माडू और गोलकुण्डा के कलाकारों के हाथों चित्रित हुई थीं।
राजपूत दरबार में संस्कृत और हिन्दी की कई पाण्डुलिपियाँ चित्रित हुई थीं और जैन चित्र उसी तरह गुजरात और राजस्थान में बन रहे थे। उस समय बादशाह अकबर ने कलाकारों के लिए बहुत बड़ा स्थान तैयार करवाया और कलाकार दूर-दूर से आगरा आने लगे, भारत की राजधानी में।
अकबर के इस बहुत बड़े ‘तस्वीरखाना’ में से जो पहली किताब तैयार हुई वह थी—तोतीनामा।
अकबर की सरपरस्ती में जो बहुत बड़ा काम हुआ, वह था—हमज़ानामा। यह हजरत मोहम्मद के चाचा अमीरहमज़ा के जंगी कारनामों की दास्तान है जो चौदह जिल्दों में तरतीब दी गयी। हर जिल्द में एक सौ चित्र थे। यह सूती कपड़े के टुकड़ों पर चित्रित की गई थी और इसे मुकम्मल सूरत देते हुए पन्द्रह बरस लगे।
‘जरीन-कलम़’ का अर्थ है सुनहरी कलम। यह एक किताब थी जो अकबर बादशाह ने कैलीग्राफी़ के माहिर एक कलाकार मुहम्मद हुसैन अल कश्मीरी को दी गई थी।
‘अम्बरी क़लम़’ भी एक किताब थी जो अकबर ने अब्दुल रहीम को दिया था। महाभारत, रामायण, हरिवंश, योगवाशिष्ठ और अथर्ववेद जैसे कई ग्रंथों का फारसी से अनुवाद भी बादशाह अकबर ने कराया था।
‘रज़म-नामा’ महाभारत फारसी अनुवाद का नाम है जिसका अनुवाद विद्वान ब्राह्मणों की मदद से बदायूँनी जैसे इतिहासकारों ने किया था, पन्द्रह सौ बयासी में और उसे फारसी के शायर फ़ैजी ने शायराना जुबान दी थी।
‘राज कुँवर’ किसी हिन्दू कहानी को लेकर फ़ारसी में लिखी हुई किताब है जिसके लेखक ने गुमनाम रहना पसंद किया था। इसकी इक्यावन पेण्टिंग सलीम के इलाहाबाद वाले तस्वीर खाने में तैयार हुई थीं।
‘बादशानामा’ शाहजहाँ के राज को लेकर अफदाल क़रीम लाहौरी की लिखी हुई वह किताब है जो औरंगजेब की बगावत ने पूरी नहीं होने दी थी।
‘ख़बरनामा’ इब्न हसन की लिखी हुई अली के कारनामों को बयान करती पुस्तक है जिसकी प्रतिलिपि मूलचन्द मुलतानी ने तैयार की थी। इसमें एक सौ छत्तीस मिनिएचर्स (भित्तिचित्र) हैं जो अफदाल हकीम मुल्तानी ने तैयार किये थे। मुल्तान में तैयार हुई इस पुस्तक के चित्रों के लिए बहुत-सा सोना और चाँदी इस्तेमाल किया गया था।
‘कारनामा-ए-इश्क़’ लाहौर के एक खत्री राय आनन्दराम की फ़ारसी में लिखी हुई किताब थी जिसके चित्र बनाते हुए उस वक़्त के मशहूर कलाकार गोवर्धन को पाँच साल लगे थे।
‘दस्तूर ए हिम्मत’ 1685 में लिखी हुई मुहम्मद मुराद की किताब थी जिसमें अवध के राजा कामरूप की और सीलोन की शहजादी कामलता की कहानी है। जिन्हें सपनों में एक दूसरे का दीदार हुआ था। राजा उसे खोजता हुआ आखिर सीलोन पहुँच जाता है और कामलता भी कामरूप को पहचान लेती है। इसकी चित्रकारी मुर्शिदाबाद में हुई, 1760 में। हर पृष्ठ पर बहुत सा सोना इस्तेमाल किया गया।
‘रागमाला’ के चित्रण में मुगल की दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मुगल दरबार के राजपूतों ओहदेदारों के कारण आगरा के तस्वीर खाने में यह पुस्तक तैयार हुई जिसमें रागों के परिवारों का ब्यौरा है। हर राग की पाँच पत्नियाँ (रागिनियाँ), और आगे उनके राग पुत्र हैं।
ब्रिटिश लाईब्रेरी लन्दन में देवचित्रों की दो एलबम हैं, जिनके चौंसठ चित्र अठारहवीं सदी के आखिर में लखनऊ के कलाकारों ने तैयार किये थे। हर चित्र के हाशिये पर सोने-चाँदी के पत्ते बनाये गये थे। ये दो एलबम दो लाख सड़सठ हज़ार एक सौ अठ्ठावन पौण्ड में बिके थे।
अठारहवीं शताब्दी के खत्म होने पर हस्तलिपियों की पाण्डुलिपियाँ बनाने की परम्परा भी खत्म हो गयी। तब कलकत्ता में प्रेस लग गया था जिसने किताबों की सूरत बदल दी।
बात दो हज़ार साल पहले की
‘अब जब जीसस का जन्म हुआ
हैरोड के राज में
देखो ! तीन आलम पूरब से चलकर
जेरुसलम आये
कहते-
वो जो जन्म से बादशाह है, वो कहाँ है ?
हमने पूरब दिशा में रहते हुए
उसका सितारा देखा है
और अपनी अकी़दत पेश करने आये हैं.......’
मैथ्यू की ऐतिहासिक किताब के ये लफ़्ज, फ़िदा हसनैन ने अपनी इस किताब में दिये हैं जो जीसस की जिन्दगी को लेकर खोज में उतरी हुई है....
किताब का नाम है-‘फ़िफ्त़ गॉस्पल’, ये फिदा हसनैन और देहन लैबी ने मिलकर लिखी है...
कहते हैं-यह खबर जब वक़्त के राजा तक पहुँची थी, उसने पूरब दिशा से आये तीनों आलिमों को बुलाया पता किया क्या वो सचमुच उसके राज में पैदा हुए उस बच्चे को देखने के लिए आए हैं जो किसी वक़्त यहूदियों का राजा होगा। इससे राजा के मन में खौफ़ आया कि उसका राज उसके हाथों से चला जाएगा। उसने तीनों से कहा-अच्छा जाओ ! तलाश करो ! पता चले तो मुझे आकर बता देना।
वो तीनों पेलेस्टीन में उस तारे की दिशा देखने लगे, जिसे देखकर वो पूरब से इस दिशा की ओर आये थे। उस वक़्त देखा, वो तारा एक नगर बैथेलेहम के ऊपर दिखाई दे रहा था। वे तीनों उस नगर चले गये, घर तलाश किया, बाल जीसस को देखा, पहचाना, और बच्चे के सामने झुककर उसे अपना सम्मान पेश किया। वो लोग साथ ही कुछ सोना, धूप और सुगन्धित सामग्री लाये थे, वो सब बच्चे को अर्पित किया और खुशी में झूमते से अपने देश लौट गये...
अनुमान किया जाता है कि वे तीनों बौद्ध थे, तन्त्र विद्या के ज्ञाता..
भारत से मध्य एशिया के कई देशों का रास्ता बौद्ध लोग जानते थे। वे बुद्ध मत को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई बरसों से देश-देश में जा रहे थे। कई देशों में उनके बनाये हुए मठ भी मिलते हैं....
फ़िदा हुसनैन ने लिखा है कि सितारों का इल्म रखनेवाले मैगी लोगों का ज़िक्र कश्मीर में लिखे गये ‘भविष्य महापुराण’ में भी मिलता है...
बौद्ध लोगों की नज़र में यह एक नये बुद्ध का जन्म हुआ था-
वो धरती जहाँ जीसस का जन्म हुआ, रोमन हुकूमत के अधीन थी, और यहूदी लोग इन्तज़ार कर रहे थे कि ख़ुदा उनकी मदद ज़रूर करेगा और किसी मसीहा को भेजेगा। वो ऐसे किसी बच्चे के जन्म का इन्तज़ार ही कर रहे थे।
ज़ाहिर है कि वक़्त का बादशाह ऐसे बच्चे के जन्म का पता लगाकर उस बच्चे का कत्ल करवा देना चाहता था। इसलिए उसके जासूस सब घरों पर नज़र रख रहे थे।....
हैरोड के राज में
देखो ! तीन आलम पूरब से चलकर
जेरुसलम आये
कहते-
वो जो जन्म से बादशाह है, वो कहाँ है ?
हमने पूरब दिशा में रहते हुए
उसका सितारा देखा है
और अपनी अकी़दत पेश करने आये हैं.......’
मैथ्यू की ऐतिहासिक किताब के ये लफ़्ज, फ़िदा हसनैन ने अपनी इस किताब में दिये हैं जो जीसस की जिन्दगी को लेकर खोज में उतरी हुई है....
किताब का नाम है-‘फ़िफ्त़ गॉस्पल’, ये फिदा हसनैन और देहन लैबी ने मिलकर लिखी है...
कहते हैं-यह खबर जब वक़्त के राजा तक पहुँची थी, उसने पूरब दिशा से आये तीनों आलिमों को बुलाया पता किया क्या वो सचमुच उसके राज में पैदा हुए उस बच्चे को देखने के लिए आए हैं जो किसी वक़्त यहूदियों का राजा होगा। इससे राजा के मन में खौफ़ आया कि उसका राज उसके हाथों से चला जाएगा। उसने तीनों से कहा-अच्छा जाओ ! तलाश करो ! पता चले तो मुझे आकर बता देना।
वो तीनों पेलेस्टीन में उस तारे की दिशा देखने लगे, जिसे देखकर वो पूरब से इस दिशा की ओर आये थे। उस वक़्त देखा, वो तारा एक नगर बैथेलेहम के ऊपर दिखाई दे रहा था। वे तीनों उस नगर चले गये, घर तलाश किया, बाल जीसस को देखा, पहचाना, और बच्चे के सामने झुककर उसे अपना सम्मान पेश किया। वो लोग साथ ही कुछ सोना, धूप और सुगन्धित सामग्री लाये थे, वो सब बच्चे को अर्पित किया और खुशी में झूमते से अपने देश लौट गये...
अनुमान किया जाता है कि वे तीनों बौद्ध थे, तन्त्र विद्या के ज्ञाता..
भारत से मध्य एशिया के कई देशों का रास्ता बौद्ध लोग जानते थे। वे बुद्ध मत को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई बरसों से देश-देश में जा रहे थे। कई देशों में उनके बनाये हुए मठ भी मिलते हैं....
फ़िदा हुसनैन ने लिखा है कि सितारों का इल्म रखनेवाले मैगी लोगों का ज़िक्र कश्मीर में लिखे गये ‘भविष्य महापुराण’ में भी मिलता है...
बौद्ध लोगों की नज़र में यह एक नये बुद्ध का जन्म हुआ था-
वो धरती जहाँ जीसस का जन्म हुआ, रोमन हुकूमत के अधीन थी, और यहूदी लोग इन्तज़ार कर रहे थे कि ख़ुदा उनकी मदद ज़रूर करेगा और किसी मसीहा को भेजेगा। वो ऐसे किसी बच्चे के जन्म का इन्तज़ार ही कर रहे थे।
ज़ाहिर है कि वक़्त का बादशाह ऐसे बच्चे के जन्म का पता लगाकर उस बच्चे का कत्ल करवा देना चाहता था। इसलिए उसके जासूस सब घरों पर नज़र रख रहे थे।....
मिस्र में
जीसस के बाप जोज़फ़ को एक बुरा सपना आया कि ये बच्चा जीसस उससे और मैरी से
छीन लिया गया है। बच्चे को राजा के दरबार में ले जाया जा रहा है। इससे
जोज़फ़ और मैरी इतने फिक्रमन्द हुए कि उसी रात वहाँ से निकलकर मिस्र की ओर
चल दिये....
कुछ दिनों बाद राजा का फ़रमान हुआ कि उसके राज में पैदा हुए सब छोटे बच्चे मरवा दिये जाएँ। ये कत्लेआम हर माँ-बाप के लिए भयानक जुल्म का समय था। कुछ मां-बाप अपने-अपने बच्चे को छिपाकर किसी-न-किसी दूसरे देश की ओर निकल गये, लेकिन सरहद पर पहरा था, इसलिए बहुत लोग निकल नहीं पाये...हर जगह कत्लेआम होने लगा।
मिस्र के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसी जगह थी, जिसे बूटी बाग़ कहा जाता था-हर्बल गार्डन। वहां कोई चार हज़ार ऐसे लोग रहते थे, जो बड़ी सादी ज़िन्दगी जीते थे, और पेड़-पौधों का इल्म रखते थे, जिनसे वे कई तरह की दवादारू बनाना जानते थे। कहते हैं कि मैरी और जोज़फ़ ने बच्चे को लेकर वहीं पनाह ली...
उस बूटी बाग में अभी तक अंजीर का वो बहुत बड़ा पेड़ का़यम कहा जाता है जिसके एक ओर बड़ी सी खुली गहरी जगह थी, जिसके अन्दर राजा के जासूसों से डरकर बच्चे को छिपा दिया जाता था...
मोसिस के वक़्त उसकी अगवाई में एक क़बीला ऐसा बना था, बड़े भले और रहमदिल लोगों का, जो सिर्फ़ सफ़ेद कपड़े पहनते थे, पेड़-पौधों का इल्म करते थे, और उनका अक़ीदा ख़ुदा की ख़लकत को प्यार करता था। वो किसी जानवर की हत्या भी नहीं करते थे इसलिए तारीख़दानों को अनुमान होता है कि वे पश्चिम के बौद्ध सन्त थे। वही लोग थे जो हर जगह मैरी की और बच्चे की हिफा़जत करते रहे....
कुछ दिनों बाद राजा का फ़रमान हुआ कि उसके राज में पैदा हुए सब छोटे बच्चे मरवा दिये जाएँ। ये कत्लेआम हर माँ-बाप के लिए भयानक जुल्म का समय था। कुछ मां-बाप अपने-अपने बच्चे को छिपाकर किसी-न-किसी दूसरे देश की ओर निकल गये, लेकिन सरहद पर पहरा था, इसलिए बहुत लोग निकल नहीं पाये...हर जगह कत्लेआम होने लगा।
मिस्र के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसी जगह थी, जिसे बूटी बाग़ कहा जाता था-हर्बल गार्डन। वहां कोई चार हज़ार ऐसे लोग रहते थे, जो बड़ी सादी ज़िन्दगी जीते थे, और पेड़-पौधों का इल्म रखते थे, जिनसे वे कई तरह की दवादारू बनाना जानते थे। कहते हैं कि मैरी और जोज़फ़ ने बच्चे को लेकर वहीं पनाह ली...
उस बूटी बाग में अभी तक अंजीर का वो बहुत बड़ा पेड़ का़यम कहा जाता है जिसके एक ओर बड़ी सी खुली गहरी जगह थी, जिसके अन्दर राजा के जासूसों से डरकर बच्चे को छिपा दिया जाता था...
मोसिस के वक़्त उसकी अगवाई में एक क़बीला ऐसा बना था, बड़े भले और रहमदिल लोगों का, जो सिर्फ़ सफ़ेद कपड़े पहनते थे, पेड़-पौधों का इल्म करते थे, और उनका अक़ीदा ख़ुदा की ख़लकत को प्यार करता था। वो किसी जानवर की हत्या भी नहीं करते थे इसलिए तारीख़दानों को अनुमान होता है कि वे पश्चिम के बौद्ध सन्त थे। वही लोग थे जो हर जगह मैरी की और बच्चे की हिफा़जत करते रहे....
जीसस की ज़िन्दगी के लापता वर्ष
ज़िलावतनी के दिनों में बच्चे को पढ़ाया भी जाता था और दूसरी शिक्षा भी दी
जाती थी। जोज़फ़ बढ़ई का काम अच्छी तरह जानता था इसलिए वो भी बच्चे को
सिखलाया गया। और जब पेसेस्टीन में राज बदल गया, उस समय जीसस बारह साल का
था। माँ-बाप उसे और अपने छोटे बच्चों को लेकर घर लौट आये। करीब एक साल
जीसस वहां मां-बाप के पास रहा, और फिर आगे इतिहास नहीं जानता कि जीसस कहाँ
चला गया....
ये जीसस की उम्र के सत्रह वर्ष थे, उसकी तेरह साल की उम्र से लेकर उनतीस साल की उम्र तक, जो लापता कहे जाते हैं...
इस किताब की खोज है कि जीसस व्यापारियों की एक टोली से मिलकर वहाँ से भारत आ गया था-रूहानी इल्म पाने के लिए। वो कई नगरों, शहरों में गया, बनारस भी, लेकिन ज़्यादा वक़्त हिमालय की पहाड़ियों में
रहा।
अब तिब्बत में कप़ड़े पर लिखी हुई ऐसी इबारत मिली है कि जीसस ने बुद्ध मत की गहराई को पाया था, और फिर उनतीस साल की उम्र में अपने देश इज़राइल चला गया था....
ये जीसस की उम्र के सत्रह वर्ष थे, उसकी तेरह साल की उम्र से लेकर उनतीस साल की उम्र तक, जो लापता कहे जाते हैं...
इस किताब की खोज है कि जीसस व्यापारियों की एक टोली से मिलकर वहाँ से भारत आ गया था-रूहानी इल्म पाने के लिए। वो कई नगरों, शहरों में गया, बनारस भी, लेकिन ज़्यादा वक़्त हिमालय की पहाड़ियों में
रहा।
अब तिब्बत में कप़ड़े पर लिखी हुई ऐसी इबारत मिली है कि जीसस ने बुद्ध मत की गहराई को पाया था, और फिर उनतीस साल की उम्र में अपने देश इज़राइल चला गया था....
कई और पहलू
ये किताब जीसस की जिन्दगी के और पहलुओं की खोज में भी उतरती है-कुँवारी
माँ वाले चमत्कारी मसले को भी तलाशती है, प्राचीन इबारतों के हवाले भी
देती है और ये पता भी देती है कि वहाँ जीसस के देश में कई प्राचीन किताबें
जान-बूझकर जला दी गयीं या छिपा दी गयीं, और कई अदल-बदल कर दी गयीं....
लेकिन वो सबकुछ तलब वालों के लिए इस किताब के हरफ-हरफ में उतरने के लिए हैं। मैं इस किताब का ज़िक्र सिर्फ़ इस पहलू से कर रही हूँ कि इस खोज की रोशनी में देखा जा सकता है कि जीसस ने बुद्ध मत से क्या-क्या पाया और कितना समय बौद्ध मठों में गुज़ारा, और फिर सूली वाली घटना से तीन दिन बाद मित्रों, मुरीदों की मदद से जब उसके जख़्म कुछ ठीक हुए, तब वो कहां चला गया....
वक़्त उसके देश में क्यों खामोश रहा ?
ये ठीक है कि दुनिया की बादशाहत उसके लिए नहीं थी उसका अक़ीदा था कि ख़ुदा की बादशाहत हमारे अन्दर होती है.....
लेकिन वो सबकुछ तलब वालों के लिए इस किताब के हरफ-हरफ में उतरने के लिए हैं। मैं इस किताब का ज़िक्र सिर्फ़ इस पहलू से कर रही हूँ कि इस खोज की रोशनी में देखा जा सकता है कि जीसस ने बुद्ध मत से क्या-क्या पाया और कितना समय बौद्ध मठों में गुज़ारा, और फिर सूली वाली घटना से तीन दिन बाद मित्रों, मुरीदों की मदद से जब उसके जख़्म कुछ ठीक हुए, तब वो कहां चला गया....
वक़्त उसके देश में क्यों खामोश रहा ?
ये ठीक है कि दुनिया की बादशाहत उसके लिए नहीं थी उसका अक़ीदा था कि ख़ुदा की बादशाहत हमारे अन्दर होती है.....
ईशा नाथ
इस किताब ने भारत के नाथ योगियों की ‘नाथ नामावली’
खोज ली है, और उसमें दिया गया ज़िक्र दर्ज किया है-
ईशा नाथ चौदह साल की उम्र में भारत आया था। योग विद्या लेने के बाद वो अपने देश लौट गया, अपने लोगों को रूहानी इल्म देने के लिए...
‘‘दुनियावालों ने उसके ख़िलाफ़ साजिश की और उसे सूली पर लटका दिया। सूली के समय ईशा नाथ ने अपने प्राण समाधि में लगा दिये थे। वो ट्रान्स में चला गया था, जिससे लोगों ने समझा वो मर गया है। वो योगी था। उसे मुर्जा समझ कर क़ब्र में उतार दिया गया....
ठीक वही समय था, जब उसके नाथ गुरु महाचेतना नाथ ने हिमालय में बैठे हुए एक विज़न देखा-एक भयानक तकलीफ जिसमें से ईशा नाथ गुज़र रहा था। उस वक़्त महाचेतना नाथ ने अपनी स्थूल काया वहीं छोड़ दी, सूक्ष्म काया अख्तियार कर ली, और इजराइल पहुँचकर जीसस को क़ब्र से निकाला...
‘‘महाचेतना नाथ यहूदियों पर बहुत नाराज़ थे, जिन्होंने ईशा नाथ को सूली पर लटका दिया था, इसलिए अपने गुस्से का इजहार कुदरत के माध्यम से किया-उस समय भयानक बादल गरजे, बिजली चमकी सारे इज़राइल में।
‘‘चेतना नाथ, ईशा नाथ को समाधि से वापस लाये। उसके जख़्म ठीक किये और उसे भारत लौट आने के लिए कहा..ईशा नाथ ने लौटकर हिमालय के निचले हिस्से में अपना आश्रम बनाया...’’.
ईशा नाथ चौदह साल की उम्र में भारत आया था। योग विद्या लेने के बाद वो अपने देश लौट गया, अपने लोगों को रूहानी इल्म देने के लिए...
‘‘दुनियावालों ने उसके ख़िलाफ़ साजिश की और उसे सूली पर लटका दिया। सूली के समय ईशा नाथ ने अपने प्राण समाधि में लगा दिये थे। वो ट्रान्स में चला गया था, जिससे लोगों ने समझा वो मर गया है। वो योगी था। उसे मुर्जा समझ कर क़ब्र में उतार दिया गया....
ठीक वही समय था, जब उसके नाथ गुरु महाचेतना नाथ ने हिमालय में बैठे हुए एक विज़न देखा-एक भयानक तकलीफ जिसमें से ईशा नाथ गुज़र रहा था। उस वक़्त महाचेतना नाथ ने अपनी स्थूल काया वहीं छोड़ दी, सूक्ष्म काया अख्तियार कर ली, और इजराइल पहुँचकर जीसस को क़ब्र से निकाला...
‘‘महाचेतना नाथ यहूदियों पर बहुत नाराज़ थे, जिन्होंने ईशा नाथ को सूली पर लटका दिया था, इसलिए अपने गुस्से का इजहार कुदरत के माध्यम से किया-उस समय भयानक बादल गरजे, बिजली चमकी सारे इज़राइल में।
‘‘चेतना नाथ, ईशा नाथ को समाधि से वापस लाये। उसके जख़्म ठीक किये और उसे भारत लौट आने के लिए कहा..ईशा नाथ ने लौटकर हिमालय के निचले हिस्से में अपना आश्रम बनाया...’’.
कुछ क़बीला
कुश, नोहा का पोता था, हैन का बेटा, जिसके नाम से कुश क़बीला का़यम हुआ।
इस क़बीले ने बगदाद में ‘काश’ नाम का गांव बसाया। ये
लोग
पहाड़ों, दरियाओं और नगरों, वादियों के नाम अपने पूर्वज कुश के नाम पर
रखते रहे...
मैसोपोटामिया में इन लोगों का राज भी हुआ था, जहाँ के दरिया का नाम इन्होंने काशान रखा। निशापुर ईराम में इस क़बीले के लोगों ने काशमार नाम का गाँव बसाया। मध्य एशिया में गये तो मुखारा में एक गाँव कॉश बसाया। और कई जगहों पर काशमुहरा, काशबन्द जैसे गाँव बसाये। समरकन्द में काशनिहा नाम का गाँव बसाया...
मैसोपोटामिया में कई नगर मिलते हैं-काशान, काशी जैसे। ये कबीला अफगानिस्तान गया, वहाँ आबाद हुआ, तो कई स्थानों के नाम रखे-काशकार, काशहिल, काशएक काशू....
हिन्दू कुश पर्वत भी इसी कबीले के नाम पर कहा जाता है। ये बाबर था जिसने अपनी ज़िन्दगी की घटनाएँ लिखते हुए लिखा है कि ‘कश्मीर’ लफ़्ज, उसकी वादी में आकर बस गये कुश क़बीले से बना था।
मैसोपोटामिया में इन लोगों का राज भी हुआ था, जहाँ के दरिया का नाम इन्होंने काशान रखा। निशापुर ईराम में इस क़बीले के लोगों ने काशमार नाम का गाँव बसाया। मध्य एशिया में गये तो मुखारा में एक गाँव कॉश बसाया। और कई जगहों पर काशमुहरा, काशबन्द जैसे गाँव बसाये। समरकन्द में काशनिहा नाम का गाँव बसाया...
मैसोपोटामिया में कई नगर मिलते हैं-काशान, काशी जैसे। ये कबीला अफगानिस्तान गया, वहाँ आबाद हुआ, तो कई स्थानों के नाम रखे-काशकार, काशहिल, काशएक काशू....
हिन्दू कुश पर्वत भी इसी कबीले के नाम पर कहा जाता है। ये बाबर था जिसने अपनी ज़िन्दगी की घटनाएँ लिखते हुए लिखा है कि ‘कश्मीर’ लफ़्ज, उसकी वादी में आकर बस गये कुश क़बीले से बना था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book